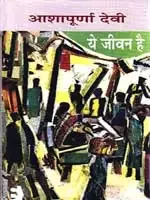|
नई पुस्तकें >> ये जीवन है ये जीवन हैआशापूर्णा देवी
|
5 पाठक हैं |
||||||
इन कहानियों में मानव की क्षुद्र और वृहत् सत्ता का संघर्ष है, समाज की खोखली रीतियों का पर्दाफाश है और आधुनिक युग की नारी-स्वाधीनता के परिणामस्वरूप अधिकारों को लेकर उभर रहे नारी-पुरुष के द्वन्द्व पर दृष्टिपात है।
ये जीवन है
हितैषी
चार वर्ष की कच्ची उम्र से जब घण्टू बाबा आदम का शिष्य था, उसी समय से उसने रोजगार पकड़ा था।
चाहे उससे दो-तीन पैसे ही जुटते हो, रोजगार तो था!
बस्ती के सारे बच्चे हाथ में टोकरी लेकर कोयला चुनने रेल लाइन के किनारे दौड़ जाते, घण्टू भी उनके पीछे-पीछे दौड़ता। उसकी कमर में बँधे तागे से लटका ताम्बे का पैसा नाचता रहता था साथ-साथ। बस्ती के ही कुछ लोग, जिनकी हालत इनसे थोड़ी अच्छी थी, यानी जो कमाऊ तो थे पर धनी नहीं थे, वे दो-चार पेसे देकर इनसे कोयला खरीद लेते। और खरीदती थीं आस-पास के गरीब गृहस्थ घरों की स्त्रियाँ। वे जलावन के नाम पर पति से पैसे लेतीं मगर काम इन पथरीले और अधजले कोयले से चलाकर कुछ पैसे बचा लेतीं।
घण्टू को प्रायः सभी पसन्द करते, क्योंकि कोयला चुनने में वह बड़े बच्चों से कम नहीं था, मगर हिसाब लगाने में एकदम बुद्धू।
एक बासी रोटी या दो सूखी डबल-रोटी के टुकड़े के बदले ही एक टोकरी कोयला उँड़ेल देता।
कुछ लोग अपने विवेक का गला घोंटकर लेन-देन का हिसाब बेठा लेते लेकिन जिसमें थोड़ा भी विवेक बाकी रहता, वे कहते, ''क्यों रे घण्टू जा रहा है, कोयले का दाम नहीं लेगा?''
घण्टू अकारण दाँत निपोरकर हँसता हुआ कहता-''हिः।''
दो, तीन-जिसे जो सही लगता, उतने पैसे दे देता।
पैसे मिलते ही घण्टू दौड़ जाता भूँजावाले की दुकान पर।
उन गृहस्थ स्त्रियों में ही किसी ने एक दिन एक फटा हुआ हाफपैण्ट देकर उससे कहा, ''ऐ घण्टू इसे पहन ले। छिः। इतना बड़ा लड़का नंगा ही घूमता है, शर्म नहीं आती?''
शर्म का एहसास अबतक उसे था ही नहीं। मगर इस प्रश्न को सुनकर घण्टू
के चेहरे पर शर्म की लाली फैल गयी। सर झुकाकर बोला, ''बुढ़िया देती ही नहीं।''
''अच्छा, मैं दे रही हूँ ले ले।''
घण्टू ने हाफ़पैण्ट ले लिया और काफी संघर्ष कर पहन भी लिया। दोनों पाँव एड़ी को छूने को और कमर को एक कपड़े के टुकड़े से बाँधना पड़ा। फिर भी घण्टू की खुशी का पारावार नही था।
सभ्यता की ओर यही उसका पहला क़दम था।
बुढ़िया कहकर जिसे घण्टू धिक्कार रहा था वह उसकी दादी थी। बेटा-बहू दोनो चल बसे थे। और पोता उसके लिए एक बला से अधिक नही था। उसका परिवार, उसकी बेटी और बेटी के बच्चों से ही बनता था। बड़ी दया करके वह सुबह-शाम दो मुट्ठी अन्न उसके आगे डाल देती। घण्टू के लिह! उतना ही पर्याप्त था।
सारे बदन पर काई-सी जमी रहती थी, दाँतो पर धब्बे, बहते हुए कान-मगर घण्टू का जीवन मज़े में कट रहा था। अब हाफपैण्ट पहनकर खुशी और बढ़ चली थी। अपने को तीसमारखाँ समझने लगा।
धीरे-धीरे हाफ़पेण्ट उसकी चमड़ी पर जमकर बैठ गया।
पता नहीं कैसे क्या हुआ, एक दिन घण्टू हाफपैण्ट पहने इठला रहा था कि उसकी बुआ फूलमणि को उसके रोजगार का ख्याल आया। बस लगी उसके कान जोर से खींचकर पूछने, ''ए छोरा! कोयले के पैसे का क्या करता है रे?''
आ, आ कर अपने कान वापस खीचते हुए घण्टू बोला, ''मारती क्यों हो? झालचना खाता हूँ।''
''मारूँ नही? तो पूजा करूं? राक्षस जैसे थाली भर-भरकर दिन में दो बार खाता है, फिर भी पेट की आग नहीं बुझती? मुफ्त का भात आता है क्या? कल से पैसे लाकर मुझे देना।''
''नहीं।'' गर्दन झुकाकर घण्टू बोला।
मगर इधर जवाब निकला उधर बुआ का एक और थप्पड़! उसकी झुकी गर्दन सीधी हो गयी।
''अरे! मुँह पर जवाब भी देने लगा है? कल से मत खाना। मैं भी देखती हूँ दादी कितने प्यार से खिलाती है।''
कहने की ज़रूरत नहीं, इस जिद की लड़ाई में हार गया घण्टू। एक दिन भोजन नहीं मिला तो चकराकर गिर गया वह। भूँजावाले की दुकान वह कमी पूरी न कर सकी। बुआ के आगे स्वीकार करना पड़ा कि कोयले के पैसे वह मुड़ी-चने खाकर बर्बाद नहीं करेगा बल्कि सारे पैसे बुआ के हाथों में लाकर दे देगा।
मगर अगले दिन सुबह ''तू शैतान है, तेरा क्या भरोसा।'' कहकर बुआ ने अपनी दम वर्षीया बेटी को चौकीदारी करने के लिए घण्टू के पीछे भेज दिया।
कोयला वह भी चुनती थी पर वाचाल हो गयी थी। इसलिए बस्ती के तेरह-चौदह वर्ष के लड़कों के साथ चक्कर काटती थी। ममेंरे भाइ पर उसका ध्यान नहीं जाता था। माँ का निर्देश पाकर घण्टू की निगरानी के बहाने उसकी अभिभाविका बन बैठी।
अपने साथ घण्टू को लेकर घर-घर जाती, आसपास की बहुओं के साथ कोयले का मोलभाव करती और याद दिलाती रहती कि घण्टू को बुद्धु समझ अब तक लोग उस लूटते रहे। जब दाम न जंचता तो फिर घण्टू को लेकर झटके से बाहर आ जाती।
परिणाम यह हुआ कि अब तक जो एक-दो बासी रोटी, सूखी ड़बल रोटी के टुकड़े, दो मीठी बातें नसीब हाती थी, वह भी वन्द हौ गयी। जो पहले प्यार दिखाने थे, वे बोलने लगे, ''देखो इस छोरे को। खुद से नइतं वन पड़ा तो लड़ने के लिए एक सरदार पकड़ लाया है।''
घण्टू के सुख के दिन लद गये।
अब पहले जैसा स्वच्छन्द विचरण बन्द हो गया, अपनी मर्ज़ी से काम पर जाना बन्द हो गया। अब सवेरा हुआ कि बड़ी-सी टोकरी लेकर निकलना पड़ता और दिन भर काम करना पड़ता।
जरा अनमना होकर रेलगाड़ी का आना-जाना देखने लगा या किसी गाय के पीछे-पीछे 'हट-हट' कर दौड़ा या पल-दो-पल पैर पसारकर बैठ गया कि फुफेरी बहन बतासी दो-चार हाथ जड़ देती।
बाँस से दबिया तगड़ी होती है। धूप से तेज होती है बालू की गर्मी।
बुआ की भारी हथेली के थप्पड़ से उसकी बेटी की छोटी-सी हथेली की मार ज्यादा पीड़ा छोड़ जाती।
उस पीड़ा से पीड़ित एक दिन घण्टू की अक्ल का दरवाजा खुल गया। सोचा उसने-'मैं किसका हूँ? कौन है मेंरा? दो जून भात के लिए अगर पैसे ही देने पड़ें तो दादी और बुआ के पास क्यों पड़ा रहूँ-बतासी की गुलामी अब और नहीं।
इसलिए एक दिन बतासी के देखने ही देखते चलती हुई ट्रेन पर उछलकर चढ़ गया घण्टू।
लोकल ट्रेन अकारण ही जब-तब यहाँ-वहाँ रुक जाती है। शरारती बच्चे इन्हीं गाड़ियों से आना-जाना करते है। यह कोई नयी बात नहीं है। मगर जब गाड़ी चल पड़ी और घण्टू उतरा नहीं तब बतासी फटे बाँस के से स्वर में चीख उठी, ''अरे मुँहजले, नालायक उतर आ, गाड़ी चलने लगी है।''
घण्टू डरा नहीं। बतासी चिल्लाने लगी, ''लौटेगा तो पता चलेगा, क्या हाल करती है माँ तेरा, तुझे यम-द्वार पहुँचाकर रहेगी।''
इतने डराने-धमकाने का भी घण्टू पर कोई असर नहीं हुआ बल्कि वह खिड़की से बाहर मुँह निकालकर अपनी जीभ और अँगूठे दिखाकर बतासी को चिढ़ाने लगा।
उसी पल बतासी समझ गयी कि घण्टू अब वापस नहीं आएगा।
हाँ! फिर वह अपने जन्मस्थान पर वापस नहीं लौटा। महज सात वर्ष का घण्टू निरंकुश, स्वाधीन हो गया।
स्वेच्छानुसार मनचाहे स्टेशन पर उतर गया।
स्टेशन का नाम मालूम नही था और मालूम करने की इच्छा भी नहीं थी। किसी दिन चाय की दुकान से माँगकर थोड़ी-सी चाय-रोटी खा लेता तो कभी स्टेशन के होटल के पास जाकर घण्टों खड़ा रहने पर बचा-खुचा कुछ मिल जाता।
फिर भी बड़ा खुश था।
रोज़-रोज टोकरी लेकर कोयले चुनने के लिए दौड़ना तो नहीं पड़ता। दादी, बुआ और बतासी की डाँट तो नही सुननी पड़ती। यह कोई छोटा-मोटा सुख था क्या?
इस सात वर्ष की उम्र में ही दिव्य ज्ञानी घण्टू समझ गया कि सर के ऊपर किसी ऊपरवाले का न होना ही चरम सुख है।
मगर सुख की अनुभूति क्षणिक ही होती है।
इस दुःखमय धराधाम पर सुख जैसी नश्वर चीज़ और है भी क्या?
स्टेशन पर चाय का दुकानदार एक दिन उसे बुलाकर अकारण ही बरस पड़ा, ''क्यों रे? रोज़-रोज़ मुफ्त की रोटी तोड़ेगा क्या? कुछ काम-धाम किया कर।''
खाने को कुछ खास मिलता नहीं था, इसलिए मुँह चिढ़ाकर घण्टू बोला, ''एः। बड़ा खिलाता है। ओ-हो-हो।''
दुकानदार चिढ़कर बोला, ''अरे, मेरे बाप-दादा-चौदह पुरखों के गुरुवंश का नाती है तू। मैं मर जाऊँ। तुझे पेटभर खाना नहीं दिया? अहा-हा-हा। बोल क्या दूँ तुझे?''
घण्टू के लिए ये शब्द नये थे। इसलिए उसने चिढ़कर जवाब दिया, ''सुबह-शाम भात खाने को दो तो मैं काम कर सकता हूँ।'' दुकानदार ने सोचा, बुरा ही क्या है!
पैंसे की बात तो की ही नहीं छोकरे ने, शायद मालूम ही नहीं। सिर्फ दो बार खाना देना और बदले में चाय के बर्तन धोना, केतली माँजना, और पान लगाना। दिन-रात काम लिया जा सकेगा।
उसने घण्टू के हाथ में साबुन की टिकिया थमा दी और शक नयी गंजी और नया पैण्ट लाकर दिया।
साबुन से नहा-धोकर नये कपड़े पहनकर घण्टू जिस दिन दुकान के नीचे स्टूल पर पैर लटकाकर बैठा, उसे लगा वह बादशाह है इस दुनिया का।
काम भी बुरा नहीं था।
कम-से-कम कोयला चुनने से तो सौ-गुना अच्छा था।
केवल दो जून क्यों, दिन में चार बार खाने को मिल जाता था। काम बहुत करता था। इसलिए डाँट भी कम पड़ती थी। एक तरह से कहा जाए तो हालत पहले की अपेक्षा सुखद ही थी।
मगर वही...।
वही सुख की नश्वरता!
नसीब फूटा। एक और चायवाला बहकाने लगा उसे, ''बिना मजूरी के काम क्यों करता है रे?''
घण्टू स्टूल पर बैठकर पैर नचाते-नचाते बोला, ''मजूरी लेकर क्या करूँगा? सब कुछ तो मिल ही जाता है।''
''अरे बुद्धु सब मिल जाता है, इसलिए वैसे ही मेंहनत करेगा?''
''ठीक ही तो है।''
''अभी तो ठीक है। मगर किसी दिन नौकरी से निकाल दे तो तेरे हाथ में रहेगा क्या? हवा फाँकेगा?''
''क्यों निकाल देंगे भला?''
''लो! क्यों निकाल देंगे? अरे बाबा, स्वर्ग से टपका है क्या? अरे! जब चीजों के दाम बढ़ेंगे तो तुझे खिलाना भारी पड़ जाएगा।''
''ठीक है, माँग लूँगा।'' कहकर फिर पैर नचाने लगा घण्टू।
मगर मजूरी माँगते ही हालत बिगड़ गयी। आराम हवा हो गया। मालिक ने उसकी खूब पिटाई की और धमकाया, ''देख लूँगा मैं भी कौन तुझे यहाँ पचास रुपये पगार देकर रखता है।''
घण्टू की माँग सिर्फ पाँच रुपये की थी, यह उसके मालिक को याद नहीं रहा। स्टेशन के सारे लोग तमाशा देखने लगे। उनमें वह भी खडा 'हि-हि' हँस रहा था, जिसने उसे बहकाया था।
फिर रेलगाड़ी पर चढ़ बैठा घण्टू।
बिना टिकट पहले बच गया था, मगर इस बार चैकर ने पकड़ लिया। चैकर घण्टू का चेहरा देखते ही भाँप गया कि इससे कुछ मिलना नहीं है। शायद इसीलिए उसने घण्टू की गर्दन पर दो मुक्के रसीद कर दिए फिर पूछा, ''काम करेगा?''
घण्टू होशियार हो चुका था, इसलिए बोला, ''करूँगा, मगर पगार देनी पडेगी।''
''अरे बाप रे! ये तो लगता है वसा ही है-ज़हर का पता नहीं सूप जैसा फन फैला रहा है। मैंने कब कहा कि बिना पगार के काम कराऊँगा? कितनी देनी होगी-सौ? दो सौ?''
"पाँच रुपये तो देगे न?''
चैकर को लगा, लड़का कापी काम आएगा। वह खुश हो गया। उसके साले
साहब के घर नौकर की तकलीफ थी। उसने कान पकड़कर घण्टू को उसके सुपुर्द कर दिया।
साले साहब भी रेल के कर्मचार्रो थे। छोटा-सा रेल-क्वार्टर था, ऊपर-नीचे का झमेंला नहीं था। काम भी हल्का था। उनकी पत्नी कोमल स्वभाव की थी। चार बार ही क्यों, अपने बच्चों के साथ सात बार खिलाती। वे जो कुछ भी खाते, घण्टू को भी दिया करती।
अच्छी कमीज और धोती खरीदकर दी थी। बिस्तर, मच्छरदानी, सब दिया था। घण्टू मानों सातवें आसमान में विचर रहा था!
महीने के अन्त में पगार के पाँच रुपये पाते ही उसके सारे दाँत बाहर निकल आए। उसे लगा जैसे कोई लॉटरी लग गयी है। अब पाने को बाकी ही क्या था।
मगर रुपये लेकर वह करे भी तो क्या? पैसे तो खाने पर खर्च हो सकते थे। और खाना तो उसे हरदम मिलता रहता था। इसलिए वह मालकिन से बोला, ''ये रुपये आप ही रख दीजिए।''
''मैं क्यों लूँ? तेरे पैसे तू नहीं लगा?''
''धत्! मैं कहाँ रखूँ? हवा में उड़ जाएँ या चूहा चट कर जाए, क्या ठिकाना।'' मालकिन ने हँसते-हँसते पैसे उठाकर रख दिये। पड़ोस में सबको घण्टू की सरलता की कहानी सुनाई-''कहता है, रुपये हवा में उड़ जाएँगे या चूहे चट कर जाएँगे।''
इस तरह तीन महीने बीत गये।
विधाता ने फिर एक हितैषी को घण्टू के पास भेजा। पड़ोस में किसी और के घर का नौकर था वह।
उसने पाट पढ़ाना शक किया-''मूर्खो का सरदार है तू। तुझे तो गिनना भी नहीं आता। पता भी है कितने महीने के रुपये जमा होकर कितने होते हैं?''
घण्टू लट्टू नचाते-नचाते बोला, 'माँ जी को पता है।''
''माँ जी को पता रहने से हो गया? कितने महीने से वहाँ काम कर रहा है तू?"
''क्या पता!'' उस समय थोड़ी-थोड़ी सर्दी थी।
''क्या बात है। सुन मेरी बात-जा, अपने पैसे माँग ले। कहना-मेंरे हिसाब के पैसे दे दो। मैं अँगूठी बनवाऊंगा।''
''अंगूठी?''
घण्टू को लगा जैसे वह स्वर्गलोक का गीत सुन रहा हो। खुशी से झूमकर एक चक्कर घूम गया और बोला, ''कहाँ है अगूँठी?''
''अरे बुद्धु। कहाँ होगी अँगूठी? सुनार की दुकान पर, और कहाँ! तू माँ जी
इसके बाद घण्टू को घाट-घाट का पानी पीना पड़ा हितैषियों के चक्कर में। फिर एक दिन जब पाई-पाई को मोहताज हो गया तो अपनी अँगूठी बेचने गया। पीतल को सोने के भाव बेचने की कोशिश में पकड़ा गया और जेल गया। यहाँ तक था उसका बाल इतिहास।
बड़े दिनों बाद फिर दिखाई दिया वह कोलकाता की सड़कों पर फल बेचते हुए। लम्बा-चौड़ा, गठीला नौजवान, चौड़ी छाती देखकर कोई सोच भी नहीं सकता, कितना दुःखद रहा होगा उसका बचपन। शायद सभी निर्दयी थे। इसीलिए यौवन उसपर कुछ अधिक ही सदय था।
अब जाकर आदर्श जीवन मिला है घण्टू को। आजीवन उसने इसी जीवन की कामना की थी। कोलकाता शहर में तो नाली की कीचड़ बेचकर भी पैसे मिलते, सो फल बेचकर अच्छा-खासा कमा लेता था वह।
दैनिक खर्चा देकर घण्टू होटल में खाता, जब मर्जी सिनेमा देखता, ताश के पत्तों पर जुआ खेलता, सड़क के नल पर नहा लिया करता और रात को किसी बड़े घर के 'पोर्टिको' के नीचे सो जाता था।
इससे आदर्श जीवन और हो भी क्या सकता था? घण्टू के होंठों पर या तो वीड़ी होती या फिल्मी गीतों के बोल होते थे।
जब जी करता, धन्धा छोड़कर वह सड़कों के चक्कर काटता। उधार में भोजन, पान-बीड़ी सब मिल जाता था।
हाँ, उधार सभी देते थे उसे।
वह था भी दरिया-दिल। छः पैसे का पान खाता और दस पैसे फेंक देता। एक रुपया तीन आने का पराँठा खाकर सवा रुपये तो हमेंशा ही दे देता था, उधार देता तो कभी वापस नहीं माँगता था।
ऐसे फुर्तीले बेपरवाह नौजवान से सभी प्यार करते थे।
मगर हाँ, एक मामले में घण्टू बहुत होशियार हो गया था। किसी हितैषी के चक्कर में नहीं पड़ता था।
सब कुछ लुट जाए फिर भी किसी को अपने ऊपर हुकूमत नहीं करने देता था वह।
ताश के अड़्ड़े पर एक यार ने बड़ी कोशिश की थी पट्टी पढ़ाने की। पेसे लगाकर रोजगार बढ़ाने को प्रेरित किया। कहा था, ''रुपये पर रुपया सूद। सुबह-शाम रुपये अण्डे देगा, बच्चे देगा। पैसे लगा, दुगुना करके वापस ला दूँगा। सूद पर देगा तो दस दिन में दस रुपये के सौ मिल जाएँगे।''
मगर घण्टू अटल रहा। बोला, ''नहीं यार, ऐसे ही ठीक हूँ, अण्डे-बच्चे की जरूरत नहीं। मुझे दस के सौ नहीं करने।''
मजे में था, मिलता तो खाता, नहीं मिलता फाका करता। फिर भी मस्त था। मगर अचानक एक दिन उसकी मस्त जिन्दगी को किसी की नजर लग गयी। उसे सब कुछ बेकार लगने लगा।
क्यों रोज़-रोज़ फल बेचने निकले घण्टू, क्यों होटल में जाकर खाना खाये, क्या ताश खेलकर हारे या जीते? और शाम होते ही सिनेमा हाल में क्यों जग या गुनगुनाते हुए सड़कों पर क्यों घूमता फिरे?
अबतक जिन बातों से चरम सुख प्राप्त होता था अब वही सब अर्थहीन लगने लगीं। देखने में तो कारण सामान्य जैसे थे।
रोज सड़क के पार जिस नल पर घण्टू नहाने जाता, उसी नल को रोककर एक लड़की बैठी रहती। घण्टू का भी रोज़ का काम था नल पर जाना और नल रोकना उस लडकी का। वह वहाँ बर्तन माँजती, कपडे धोती और बड़े कौशल से साड़ी मे लिपटकर नहा भी लेती।
घण्टू कुछ दिन तो सहन करता रहा, लेकिन एक दिन उससे रहा नहीं गया। बोला, ''ये तो अच्छा तमाशा है? नल का ठेका ले लिया है क्या? सिर्फ तुम्हे ही काम है और किसी को कोई काम नहीं?''
लड़की इस हमले से रत्तीभर भी नहीं घबरायी। गर्दन घुमाकर, आँखों से बिजली चमकाकर बोली, ''क्या काम है और किसी को? न बीवी, न बच्चा, न घर-बार, दो घण्टे रुक भी गये तो क्या आसमान टूट पड़ेगा?''
बरसों पहले एक बार घण्टू की आँखो में आँसू छलके थे। आज पता नहीं क्या, फिर आँखें भर आयीं। शायद एक नारी से टक्कर लेने का अनुभव नहीं था, इसलिए असहाय महसूस करने लगा। जो जीवन उसे परम-प्राप्ति का आनन्द देता आज उसी पर किसी के उठाये सवाल ने उसे जबर्दस्त तकलीफ से भर दिया।
खैर मन में जो भी हो, आँखों में रोष लेकर घण्टू फड़क उठा, ''और तुम्हारे पास सबकुछ है क्या?''
लड़की के चेहरे पर अवज्ञा और भी स्पष्ट झलकने लगी। बोली, ''है क्यों नहीं? माँ है, बाप है, भाई-बहन हैं।''
घण्टू ने मुँह चिढ़ाकर कहा, ''है तो हैं क्या करूँ? मेरा कोई नहीं है तो तुझे क्या?''
''मेरा क्या? लोग हँसते है, बुरा लगता है। एक नम्बर का बुद्ध है तू। दोस्त बाजी में हराकर तुझे ठगते हैं, उधार लेकर वापस नहीं करते, छिः!"
बस, यही बात घर कर गयी।
सोचो तो यही कारण, नहीं तो कुछ भी नहीं।
उसी दिन से गुमसुम है घण्टू।
जो घण्टू कभी दोस्तों के लिए सबकुछ लुटा सकता था, वही दोस्तों की इस निष्ठुरता से टूट गया। अब ताश के अड्डे से बुलावा आता तो घण्टू 'तबीयत ठीक नहीं,' कहकर टाल जाता। वे उधार मॉगते तो घण्टू कहता पैसे नहीं हैं।
वे कहते, ''हुआ क्या हमारे घण्टू को?'' खुद घण्टू को ही नहीं पता क्या हो गया? हाँ, मगर फिल्में अच्छी नहीं लगतीं, गुनगुनाना भी बन्द हो गया। कभी होटल जाता तो कभी नहीं।
सिर्फ नियमानुसार प्रतिदिन सुबह फल बेचने निकल जाता धीर गति से। गाँठ में बँधी पैसो की थैली मोटी होती जाती दिन-प्रतिदिन। क्यों न होती? अब रुपया सिर्फ आता था, जाता तो था नहीं।
मगर उससे क्या?
जीवन ही जब असार लगे तो पैसों से क्या लाभ।
जब वह लड़की नल के पास होती, घण्टू उधर फटकता भी नहीं, जबकि उसका सम्पूर्ण अस्तित्व चुम्बक की तरह नल की तरफ ही आकर्षित होता रहता। अपनी मनःस्थिति को समझ पाने में असमर्थ घण्टू दिन-प्रतिदिन सूखकर काँटा होने लगा। ऐसे में अचानक एक दिन वह लड़की आयी और कँटीली भौंहें तानकर बोली, ''ऐ! नल पर क्यों नहीं आता? नाराज़ है, मुझसे?''
घण्टू ने सिर हिलाया।
''फिर?''
फिर क्या, यह न बताकर अचानक घण्टू ने एक अजीब हरकत कर दी। कमर में बँधी रुपयों की थैली निकालकर उसके हाथ में दे दी और कहा, ''ले।''
वाचाल लड़की पहली बार सहम गयी। डरकर थैली फेंक दी उसने।
दो क़दम पीछे हटकर घबरायी आवाज़ में बोली, ''तेरे पैसे मैं क्यों लेने लगूँ?''
ज़मीन से धैली फिर उठाकर घण्टू निहाल-सा होकर हँसकर बोला, ''ऐसे ही क्यों लेगी? बदले में जो मेरे पास नहीं है, वह दे दे-घर-परिवार, बीवी। और इस बुद्धू की हितैषी बन जा ताकि फिर कोई इसे लूट न सके।''
0 0
|
|||||